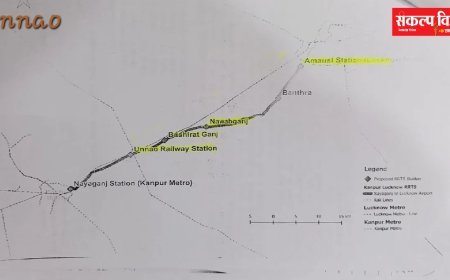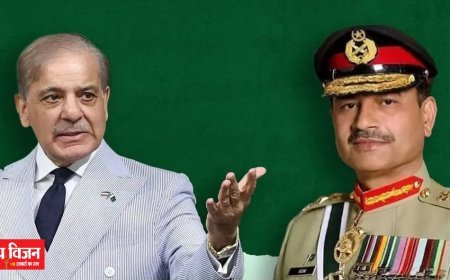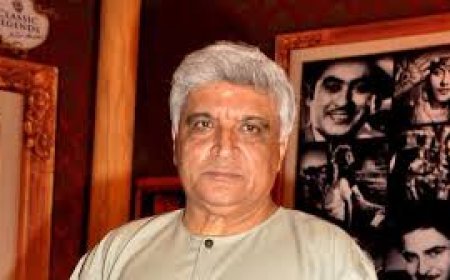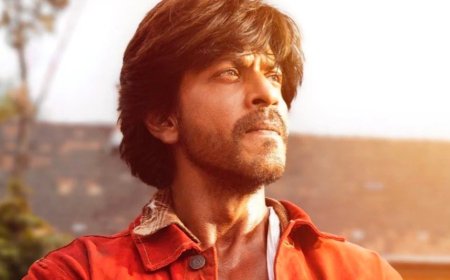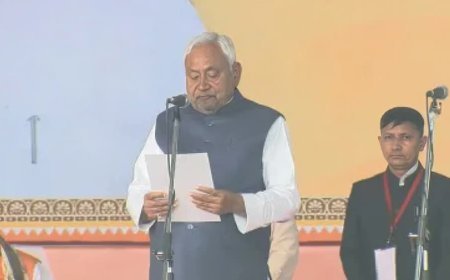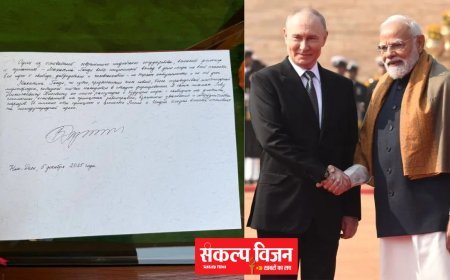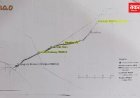सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति-राज्यपाल के लिए विधेयकों पर कार्रवाई की समयसीमा तय करने को संवैधानिक दुविधा बताया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक संवैधानिक दुविधा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सवाल उठाया कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयसीमा निर्धारित करना संविधान को न्यायिक रूप से फिर से लिखने के समान नहीं होगा, जिसमें केवल उनसे 'जितनी जल्दी हो सके' कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को एक संवैधानिक दुविधा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सवाल उठाया कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयसीमा निर्धारित करना संविधान को न्यायिक रूप से फिर से लिखने के समान नहीं होगा, जिसमें केवल उनसे ‘जितनी जल्दी हो सके’ कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की संविधान पीठ अनुच्छेद 143 के तहत विधेयकों पर मंजूरी को लेकर राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई कर रही है.
यह संदर्भ शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा 8 अप्रैल को दिए गए फैसले से उत्पन्न हुआ है, जिसने राज्यपालों और राष्ट्रपति पर विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय सीमा लगाई थी. इस फैसले के बाद इस बात पर गंभीर बहस शुरू हो गई कि क्या ऐसी समयसीमा संवैधानिक योजना को बदल सकती है.
मालूम हो कि तमिलनाडु के अलावा पंजाब, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच गतिरोध देखने को मिला है. इन राज्यों ने राजभवन पर विधायी प्रक्रिया में कथित रूप से बाधा डालने का आरोप लगाया है.
इस मामले की सुनवाई के छठे दिन पांच न्यायाधीशों की पीठ ने बार-बार इस बात पर विचार किया कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल न्यायिक रूप से निर्धारित समयसीमा का पालन करने में विफल रहे, तो संवैधानिक न्यायालय क्या उपाय अपना सकता है.
संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 जानबूझकर समयसीमा तय करने से बचते हैं
पीठ ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित हैं, जानबूझकर समयसीमा तय करने से बचते हैं.
उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 200 में प्रावधान है कि जब कोई विधेयक किसी राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है. जबकि अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर समान अधिकार प्रदान करता है. दोनों अनुच्छेदों में ‘यथाशीघ्र’ वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, बिना कोई समयसीमा निर्धारित किए.
पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायिक रूप से समयसीमाएं निर्धारित करना ‘व्यावहारिक रूप से संविधान में संशोधन करने के समान’ हो सकता है, क्योंकि दस्तावेज़ के निर्माताओं ने इन प्राधिकारियों को निश्चित अवधि से बांधने का विकल्प नहीं चुना था.
पीठ ने आगे कहा कि हालांकि, अदालतें ‘असाधारण विलंब के मामलों’ में हस्तक्षेप कर सकती हैं, लेकिन किसी मामले-विशिष्ट उपाय को कानून के सार्वभौमिक नियम में बदलना ‘एक कठिन प्रस्ताव’ है.
अदालत ने यह भी कहा कि अलग-अलग विधेयकों और संदर्भों के लिए अलग-अलग व्यवहार की आवश्यकता हो सकती है.
मंगलवार को दिनभर चली सुनवाई के दौरान एक बिंदु पर अदालत ने कहा, ‘इस मामले में एक निश्चित समयसीमा प्रदान करना संभव नहीं हो सकता क्योंकि अलग-अलग ज़रूरतें या विचार हो सकते हैं जिनके लिए अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता हो.’
इस दौरान अदालत ने समयसीमा लागू करने के परिणामों पर भी विचार किया.
इस संबंध में अदालत ने पूछा, ‘अगर समयसीमा का पालन नहीं किया गया तो क्या होगा? क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति पर अवमानना का आरोप लगाया जा सकता है? यहीं पर मुश्किलें खड़ी होती हैं.’
पीठ ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत रिट अदालतों द्वारा व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान किया जा सकता है, लेकिन अलग-अलग अधिनियमों और परिस्थितियों के लिए अलग-अलग समयसीमा की आवश्यकता हो सकती है.
‘राज्यपालों की अनिश्चितकालीन निष्क्रियता राज्य विधानसभाओं को कमज़ोर करती है’
इस मामले में तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपालों की अनिश्चितकालीन निष्क्रियता को रोकने के लिए समयसीमा ज़रूरी है, क्योंकि यह राज्य विधानसभाओं को कमज़ोर करती है और प्रभावी रूप से ‘पॉकेट वीटो’ का रूप ले लेती है.
उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि वह वास्तविकता को अनदेखा करने वाला रवैया न अपनाए, बल्कि अधिक देरी के चलते सामने आने वाली परेशानियों पर ध्यान दे.
सिंघवी ने सुझाव दिया कि ‘मान्य स्वीकृति’ समयसीमा चूक जाने के परिणामस्वरूप लागू हो सकती है. उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड के क्षमादान मामले और चुनाव आयुक्तों पर अनूप बरनवाल के फैसले जैसे उदाहरणों का हवाला दिया, जहां अदालत ने लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए संवैधानिक चुप्पी को खत्म कर दिया था.
इस धारणा को खारिज करते हुए कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक स्वीकृति रोक सकते हैं, सिंघवी ने कहा, ‘वह अंतिम मध्यस्थ या ‘सुपर सीएम’ नहीं हो सकते. कथित तौर पर असंवैधानिक विधेयक हर दिन पारित होते हैं – अदालतें उनका परीक्षण करने के लिए होती हैं. यही शक्तियों का पृथक्करण है.’
वहीं, पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने समयसीमा की मांग का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि राज्यपालों को विधेयकों को रोकने की अनुमति देने का मतलब होगा ‘जनता की इच्छा को लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राज्यपाल उसे रोकना चाहते हैं. संवैधानिक कानून का कोई भी सिद्धांत संवैधानिक तंत्र को ध्वस्त करने की अनुमति नहीं देता.’
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिंघवी द्वारा तमिलनाडु और केरल के उदाहरण दिए जाने पर आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि वे ‘1947 से’ अन्य राज्यों के आंकड़े पेश करके दिखाएंगे कि कैसे ‘संविधान का दुरुपयोग किया गया’.
इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने वकीलों को राष्ट्रपति पद के संदर्भ को पक्षपातपूर्ण मंच में बदलने के प्रति आगाह किया.
सीजेआई ने कहा, ‘हम इस मामले का फैसला इस आधार पर नहीं करने जा रहे हैं कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था सत्ता में है या थी.’
राष्ट्रपति संदर्भ में न्यायालय के समक्ष 14 प्रश्न
गौरतलब है कि इस मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मई में भेजे गए राष्ट्रपति संदर्भ में न्यायालय के समक्ष 14 प्रश्न रखे गए हैं. इनमें से कुछ प्रश्न ये हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय उन क्षेत्रों में न्यायिक रूप से प्रक्रियात्मक तंत्र तैयार कर सकता है जहां संविधान मौन है, और क्या संवैधानिक प्राधिकारियों के लिए समयसीमा तय करना संविधान निर्माताओं द्वारा उन्हें दिए गए विवेकाधिकार का अतिक्रमण है.
इससे पहले अप्रैल के फैसले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए तीन महीने और पुनः पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल द्वारा एक महीने की समयसीमा तय की थी.
पीठ ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके तमिलनाडु के 10 विधेयकों को स्वीकृत मान लिया था, और राज्यपाल की लंबे समय तक निष्क्रियता को ‘अवैध’ बताया था.
ज्ञात हो कि संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है, भले ही इसमें मौजूदा कानूनों को रद्द करना या उनमें मौजूद खामियों को दूर करना शामिल हो.
उल्लेखनीय है कि साल 2023 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पंजाब सरकार के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के ख़िलाफ़ याचिका पर अपने फैसले में यह स्पष्ट किया था, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों को लंबित रखा था.
अदालत ने कहा था कि राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.
What's Your Reaction?
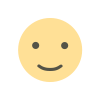 Like
0
Like
0
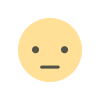 Dislike
0
Dislike
0
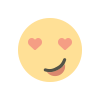 Love
0
Love
0
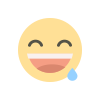 Funny
0
Funny
0
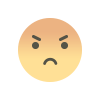 Angry
0
Angry
0
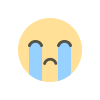 Sad
0
Sad
0
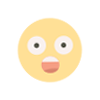 Wow
0
Wow
0